हिंदी साहित्य का रीतिकाल
परिचय
हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से रीतिकाल (1650-1850 ई.) एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। यह काल मुख्यतः काव्य परंपरा पर केंद्रित था और इसे विशेष रूप से शृंगार रस एवं नायिका-भेद की प्रधानता के कारण जाना जाता है। इस काल में कविता का प्रयोग राजदरबारों में मनोरंजन, नायिका-भेद, नीति, भक्ति और अलंकारों के प्रयोग हेतु किया जाता था।
रीतिकाल का इतिहास
रीतिकाल को हिंदी साहित्य का तीसरा प्रमुख काल माना जाता है, जो भक्ति काल के बाद और आधुनिक काल से पहले का युग है। इस काल की विशेषता यह थी कि इसमें कविता का उद्देश्य भक्ति और समाज सुधार से हटकर शृंगारिक भावनाओं को व्यक्त करना था।
रीतिकाल की कविताएँ मुख्यतः राजाओं और दरबारों से प्रेरित थीं। इस काल में कवियों ने अपने साहित्य में नारी-चित्रण, प्रेम, सौंदर्य, नायिका-भेद, अलंकारिकता और नीति विषयक शिक्षा को प्रमुखता दी। यह काल संस्कृत साहित्य और काव्यशास्त्र से अत्यधिक प्रभावित था।
इस काल का नाम "रीतिकाल" इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल के कवि काव्यशास्त्र की "रीति" (शैली) के अनुसार अपनी रचनाएँ करते थे। इनकी कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, विशेषकर संयोग और वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण मिलता है।
रीतिकाल का समय एवं नामकरण
रीतिकाल का समय लगभग 1650 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल का नामकरण "रीति" शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ "पद्धति" या "शैली" होता है। इस काल के कवियों ने संस्कृत साहित्य की रीति (शैली) को अपनाते हुए हिंदी काव्य को एक नया स्वरूप दिया।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने इस काल को "रीतिकाल" नाम दिया क्योंकि इस युग के अधिकांश काव्य संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपराओं का पालन करते थे।
रीतिकाल के कवि
रीतिकाल के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं:
- भूषण – वीर रस के प्रसिद्ध कवि, जिन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया।
- केशवदास – जिन्होंने 'रसिकप्रिया' और 'कविप्रिया' जैसी रचनाएँ लिखीं।
- बिहारी – 'बिहारी सतसई' के रचयिता, जिनकी दोहों में शृंगार रस की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है।
- मतिराम – 'रसराज' और 'रसरत्नाकर' के रचयिता।
- चिंतामणि त्रिपाठी – नीति और शृंगार पर आधारित कविताएँ लिखीं।
- देव – जिन्हें 'देव कवि' के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने नायिका भेद पर सुंदर कविताएँ लिखीं।
- पद्माकर – श्रृंगार रस के कुशल कवि।
- घनानंद – रीतिमुक्त कवियों में प्रमुख, जिन्होंने प्रेम और संवेदना की गहन अनुभूति को अभिव्यक्त किया।
- कुलपति मिश्र – श्रृंगार रस के कवि, जिन्होंने नायिका भेद पर कविताएँ लिखीं।
रीतिकाल की प्रमुख रचनाएँ
- बिहारी सतसई – बिहारी
- रसिकप्रिया – केशवदास
- कविप्रिया – केशवदास
- रसराज – मतिराम
- रसरत्नाकर – मतिराम
- श्रृंगार शतक – भूषण
- नख-शिख वर्णन – विभिन्न कवियों द्वारा रचित
- घनानंद काव्य – घनानंद
- सुजान शतक – देव
- पद्माकर ग्रंथावली – पद्माकर
रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं:
- शृंगार रस की प्रधानता – इस काल में प्रेम, सौंदर्य, नायक-नायिका भेद पर विशेष बल दिया गया।
- राजाश्रय – अधिकांश कवि राजाओं के दरबार से जुड़े थे, इसलिए उनकी रचनाओं में दरबारी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखता है।
- नायिका भेद – इस काल के कवियों ने विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का विस्तार से वर्णन किया।
- अलंकारिकता – कविताओं में अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ।
- नीति और शिक्षा – कुछ कवियों ने नीतिपरक काव्य की रचना की।
- वीर रस का प्रयोग – भूषण और अन्य वीर रस के कवियों ने युद्ध और वीरता का वर्णन किया।
रीतिकाल की विशेषताएँ
- काव्य में शास्त्रीयता – इस युग की रचनाएँ संस्कृत काव्यशास्त्र पर आधारित थीं।
- संयोग और वियोग श्रृंगार – इस काल में प्रेम के संयोग और वियोग दोनों रूपों को सुंदरता से व्यक्त किया गया।
- राज दरबारों में कवियों का संरक्षण – इस काल के अधिकांश कवि राजाओं और नवाबों के संरक्षण में थे।
- अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग – काव्यशैली को सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया गया।
- भक्ति भावना का हास – भक्ति भावना की जगह प्रेम और श्रृंगार को अधिक महत्व दिया गया।
रीतिकाल के वर्गीकरण
रीतिकाल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है:
1. रीतिबद्ध काव्य
- जो काव्यशास्त्र के नियमों का पालन करता है।
- इसमें रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का वर्णन मिलता है।
- प्रमुख कवि – बिहारी, केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम।
2. रीतिसिद्ध काव्य
- यह काव्य शृंगार रस और नायिका भेद को केंद्र में रखता है।
- प्रमुख कवि – देव, पद्माकर, बिहारी।
3. रीतिमुक्त काव्य
- इसमें प्रेम, संवेदना और मानवता के भावों को महत्व दिया गया।
- प्रमुख कवि – घनानंद, आलम, ठाकुर।
रीतिमुक्त रीतिबद्ध रीतिसिद्ध पर प्रकाश
रीतिकाल का योगदान
- हिंदी काव्यशास्त्र को समृद्ध किया।
- अलंकार, रस, नायिका भेद पर गहन अध्ययन हुआ।
- हिंदी साहित्य को परिपक्वता मिली।
- कवियों ने प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं को गहराई से व्यक्त किया।
रीतिकाल का पतन
निष्कर्ष
रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग था जिसमें श्रृंगार रस, नायिका भेद, अलंकार और राजाश्रय की परंपरा देखने को मिलती है। इस युग ने हिंदी काव्य को समृद्ध किया और संस्कृत काव्यशास्त्र को हिंदी साहित्य में सशक्त रूप से स्थापित किया। हालाँकि, इस काल में भक्ति और सामाजिक सरोकारों की कमी रही, लेकिन काव्य की कलात्मकता और सौंदर्य को नई ऊँचाइयाँ मिलीं।
मुख्य बिंदु:
1. रीतिकाल का समय: 1650-1850 ई.
2. मुख्य कवि: बिहारी, केशवदास, भूषण, देव, घनानंद आदि।
3. मुख्य विशेषता: शृंगार रस, अलंकार, नायिका भेद, राजाश्रय।
4. मुख्य रचनाएँ: बिहारी सतसई, रसिकप्रिया, रसरत्नाकर आदि।
5. समाप्ति का कारण: आधुनिक विचारधारा और यथार्थवाद का उदय।
दोस्तो रीतिकाल के बारे में आज हम लोग विस्तार से पड़े तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कॉमेंट कर के बताएं और अपने दोस्तों। को भी शेयर करे
Thank you guys 🤗

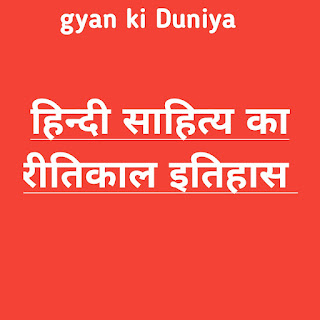



0 टिप्पणियाँ